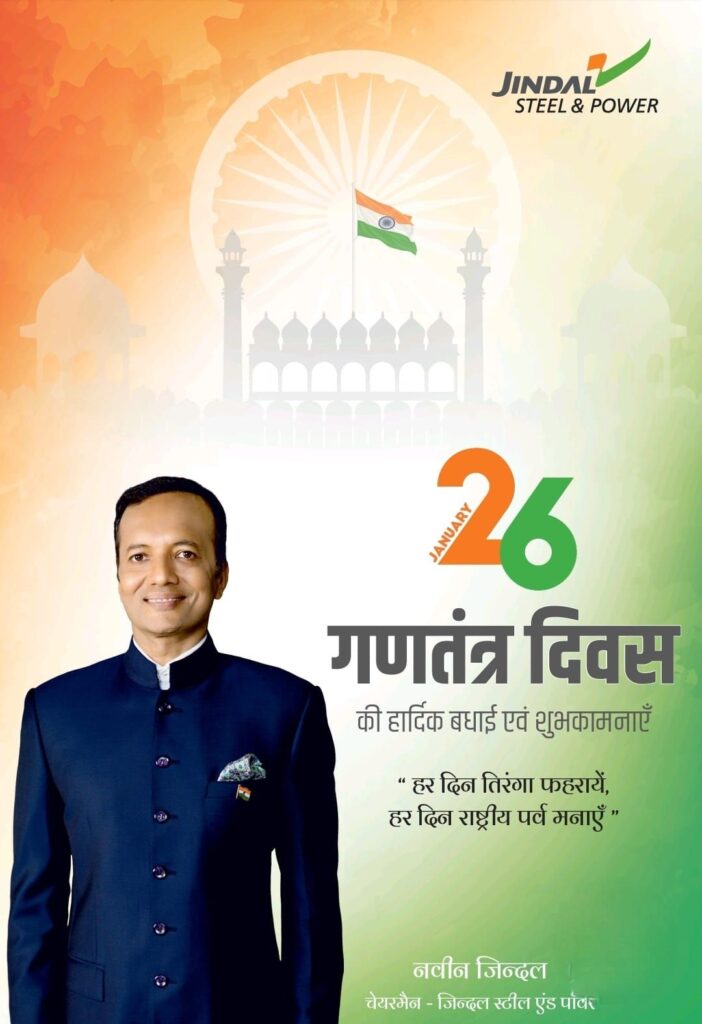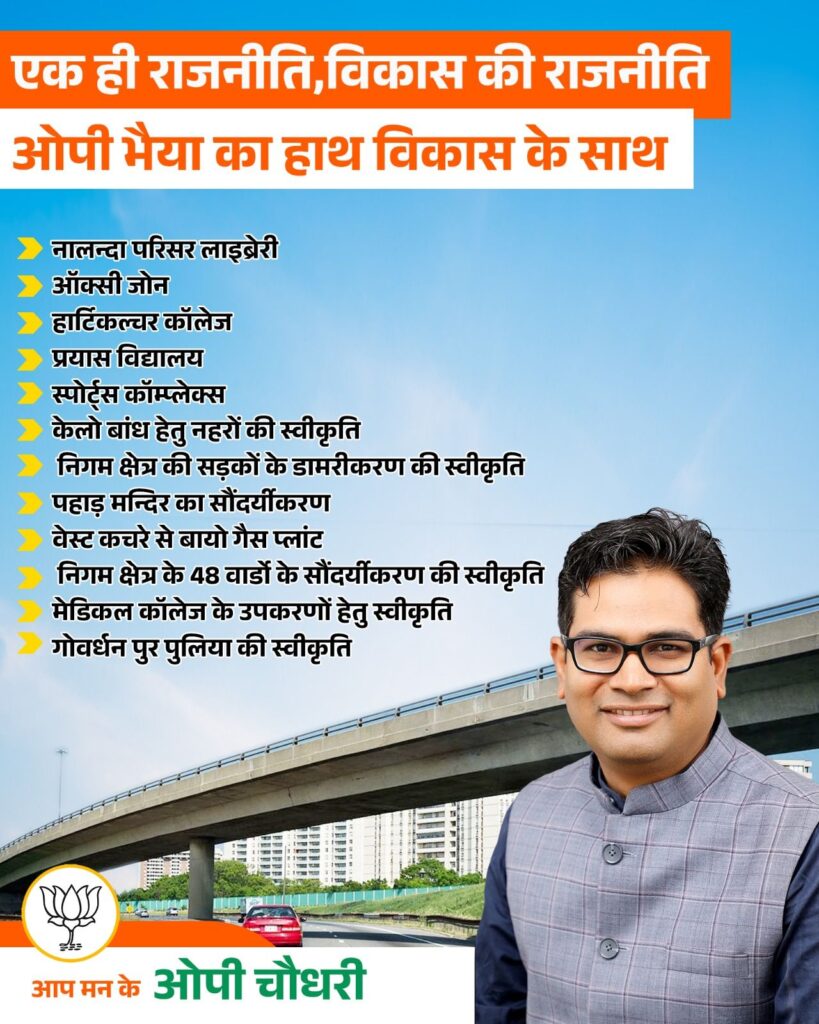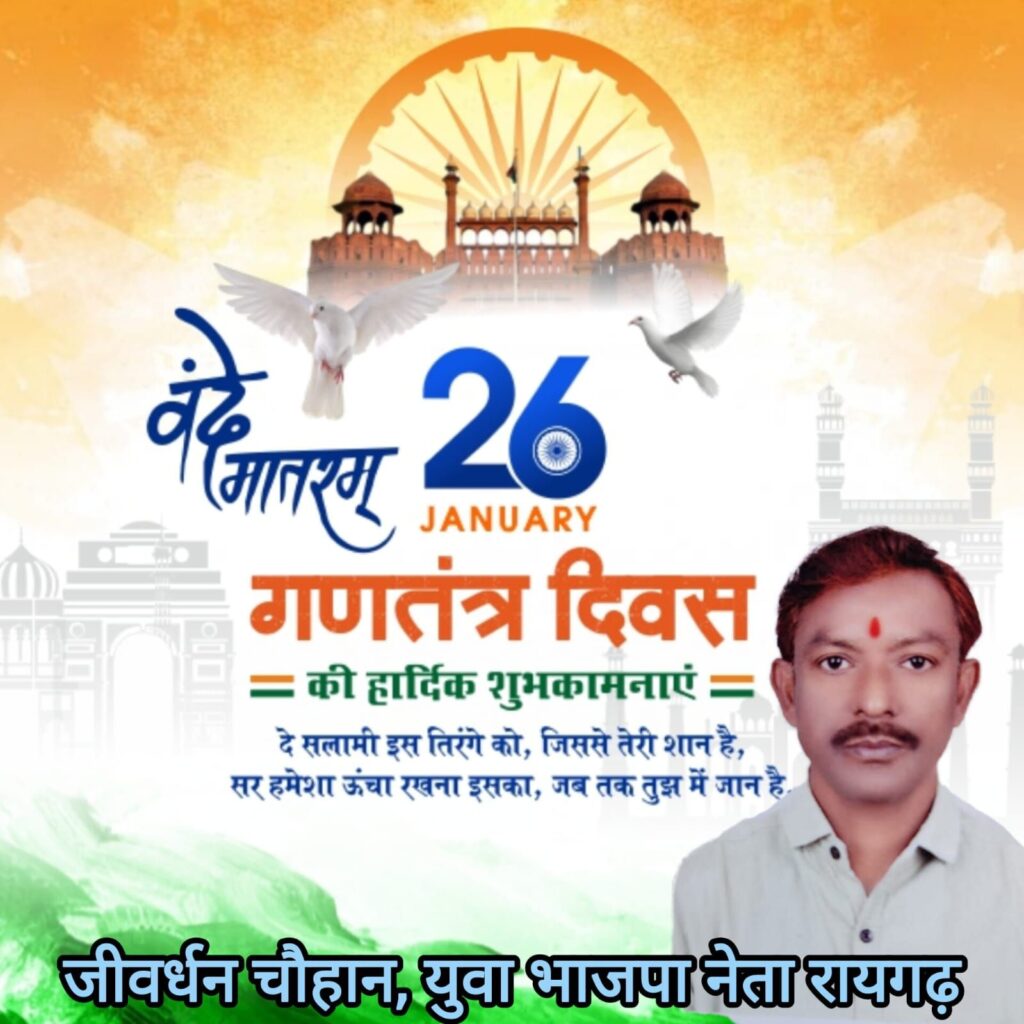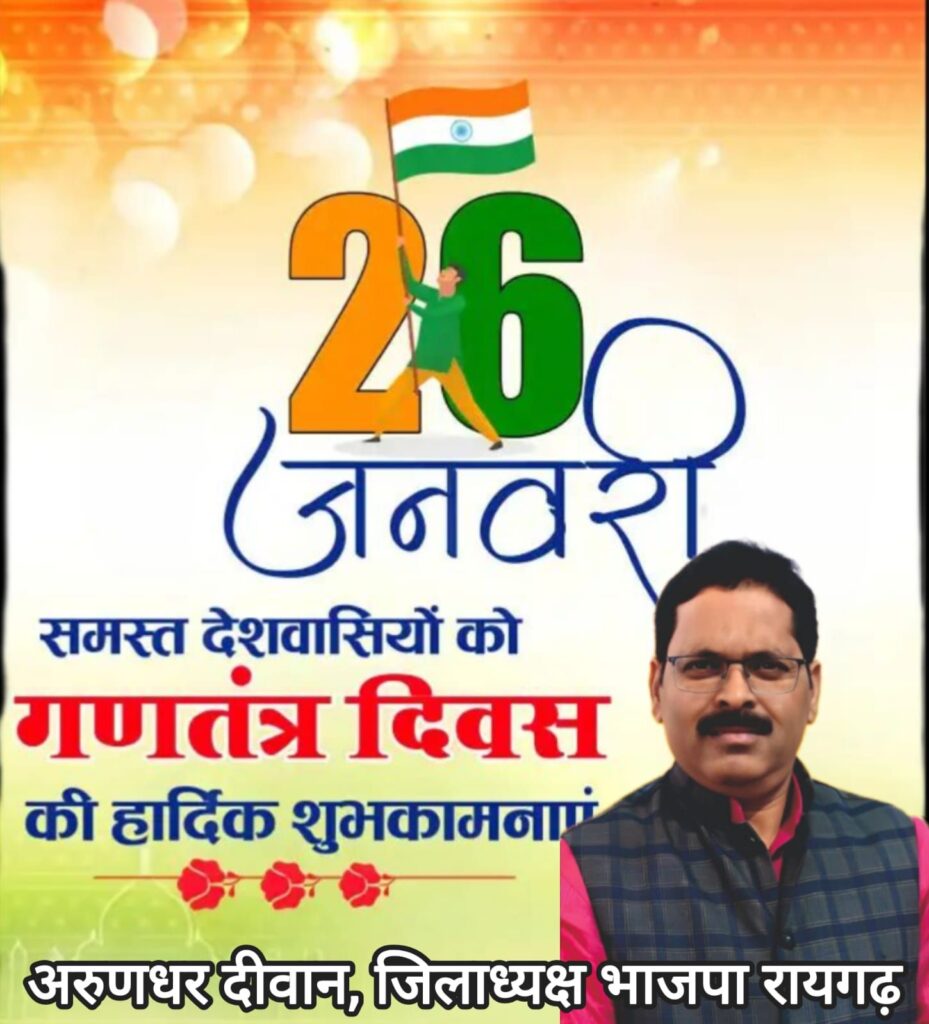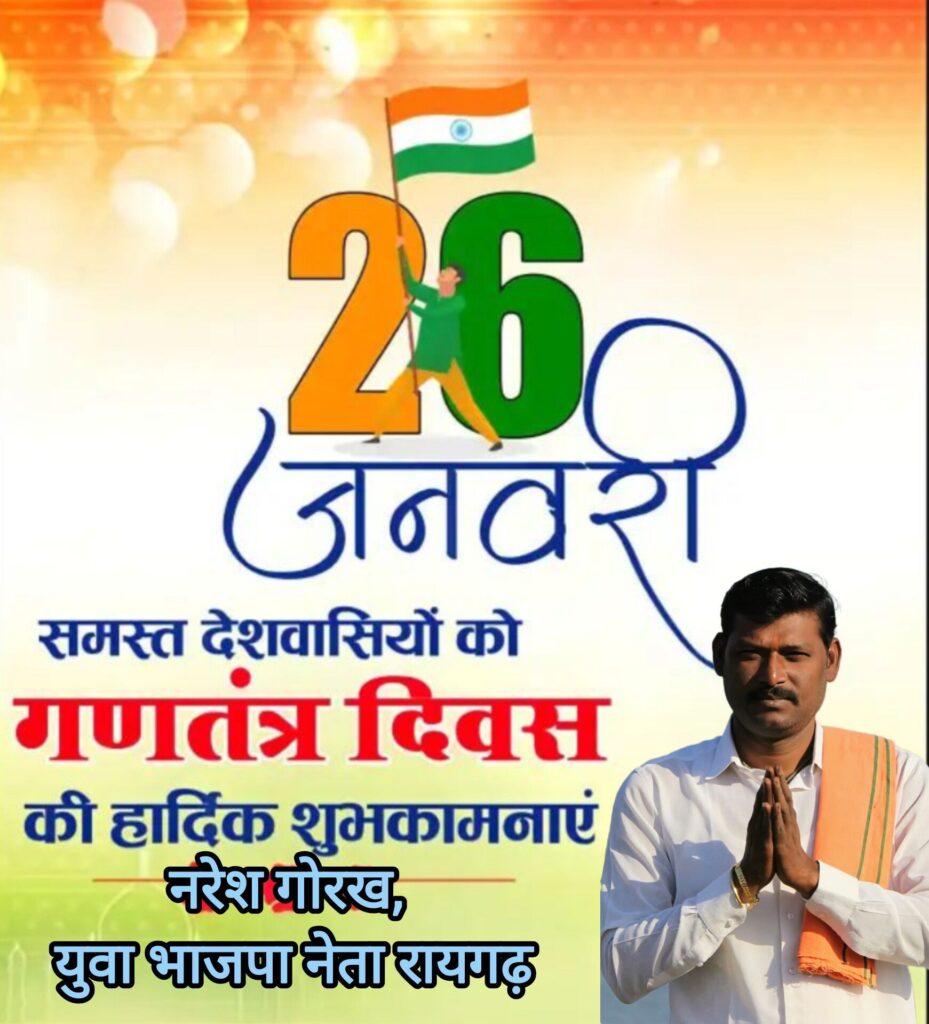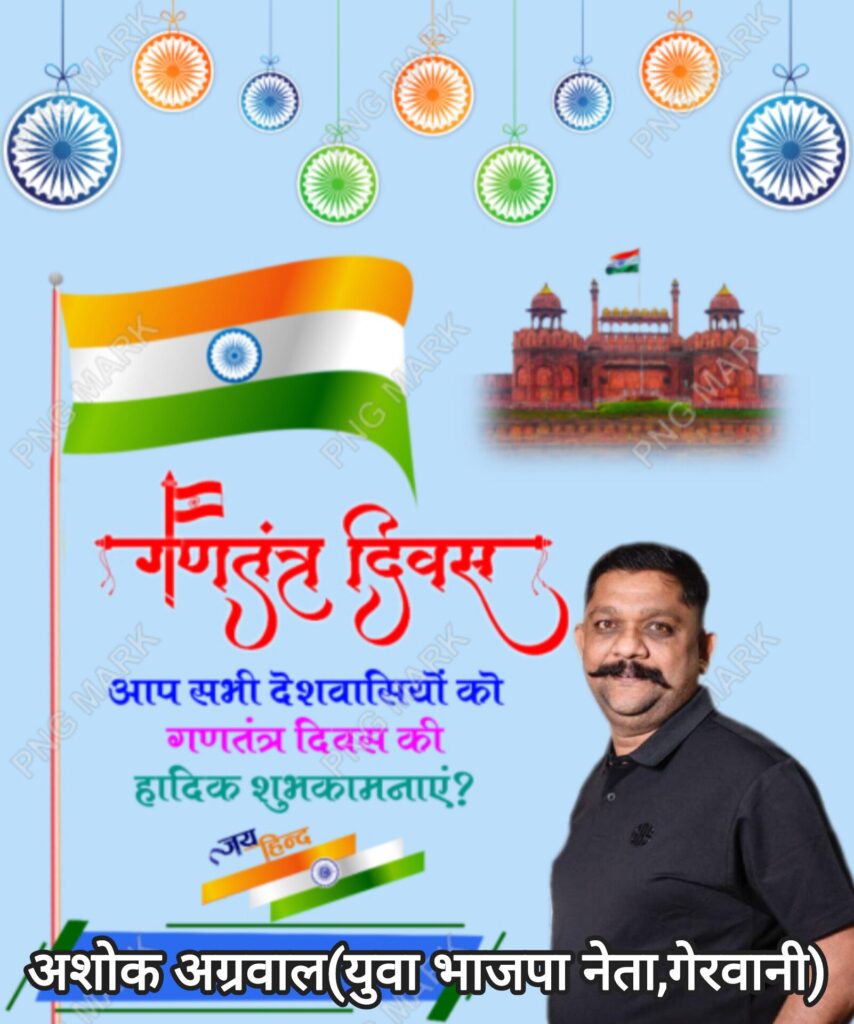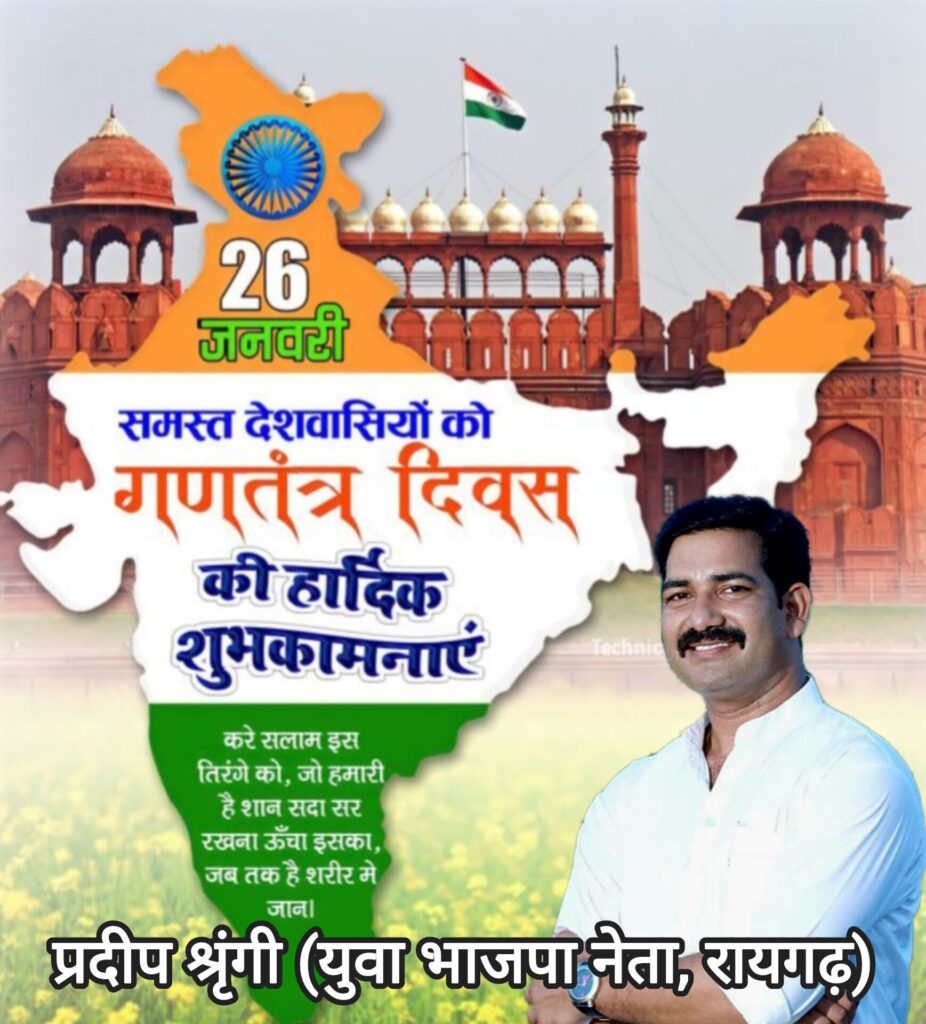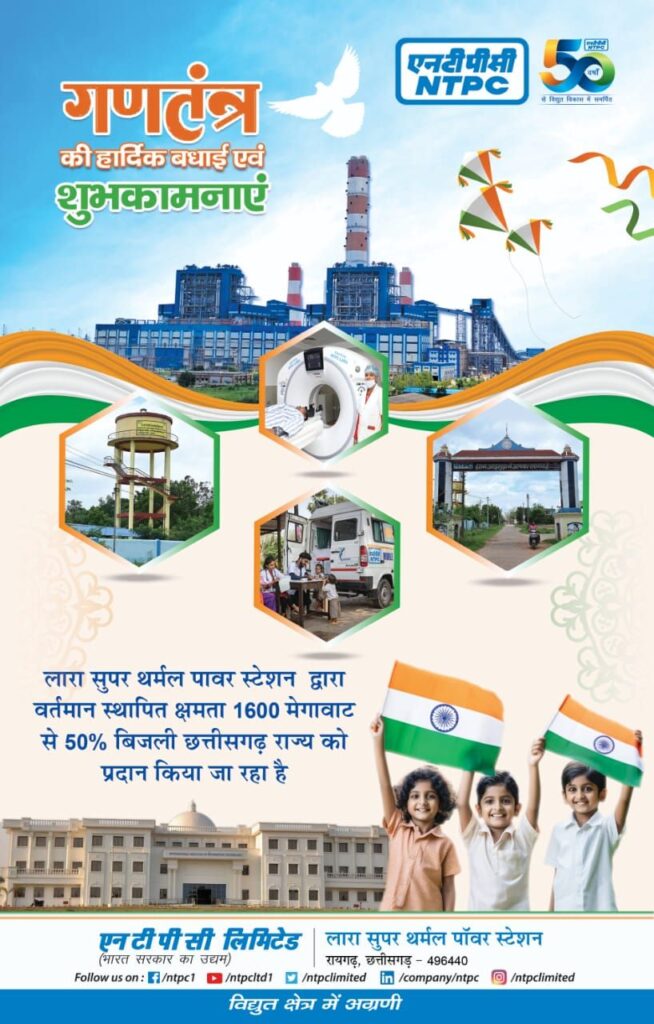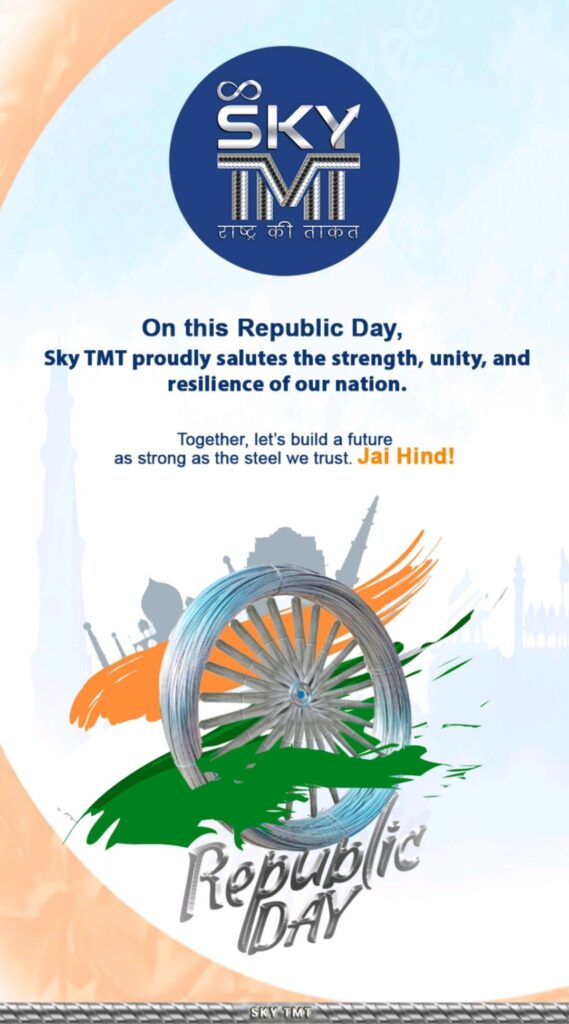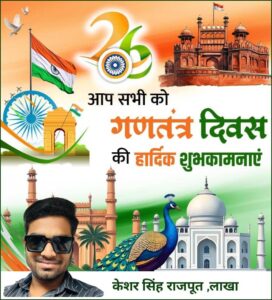देखिए क्या कहते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एसके घोष
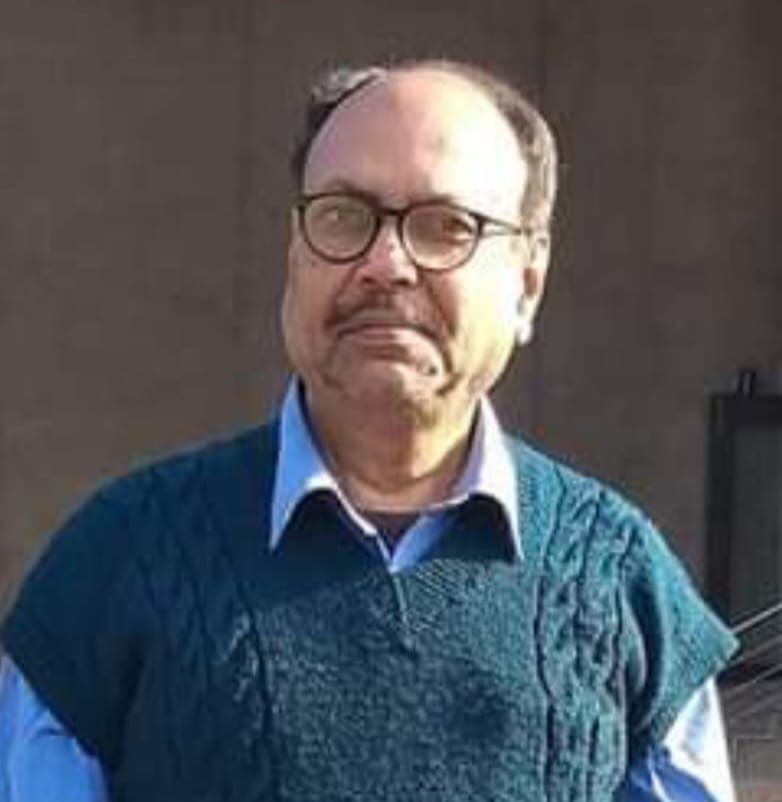
रायगढ़ (सृजन न्यूज)। शहर के सिविल लाइन निवासी और वरिष्ठ अधिवक्ता एसके घोष बताते हैं कि फायनेंस कंपनी या बैंक से अब ऋणी व्यक्ति कैसे निपटे ?

आइए जानते हैं कि फायनेंस कंपनी से ऋण अनुबंध निष्पादित करते समय मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 के अंतर्गत एक कंडिका लिखी होती हैं जिसमें कहा जाता हैं कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद होने पर मध्यस्थ याने की आर्बिट्रेटर के माध्यम से विवाद का निराकरण किया जायेगा। आर्बिट्रेटर की नियुक्ति परस्पर सहमति से की जाती है, यह तो सिद्धांत की बात है, लेकिन प्रयोग में एैसा होता नहीं हैं। बैंक एवं फायनेंस कंपनी ऋणी को नोटिस देकर एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देती हैं जो कि ऋणी व्यक्ति के निवास स्थान से 200 या 500 किलोमीटर दूर होता हैं। कुछ मामलों में देखा गया हैं कि अन्य राज्यों में आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया गया हैं। बैंक एवं फायनेंस कंपनी का यह प्रयास होता हैं कि ऋणी व्यक्ति आर्बिट्रेटर के पास तक ना पहुंच सकें, ऋणी व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रख सकें और एक पक्षीय अवार्ड पारित हो जाये। कुछ मामलों में यह भी देखने में आता हैं कि ऋणी व्यक्ति को आर्बिट्रेशन अवार्ड की काॅपी (नकल) तक उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। आर्बिट्रेशन अवार्ड की जानकारी ऋणी व्यक्ति को तब मिलती हैं जबकि फायनेंस कंपनी की ओर से मध्यस्थता एवं सुलाह कानून 1996 की धारा 36 में वसूली की कार्यवाही हेतु न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत कर दिया जाता हैं।

प्रश्न यह है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित हो गया हैं तो अब आप क्या करेंगे ? ऋणी व्यक्ति के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? मान लो कि अनसिक्यूर्ड ऋण का मामला हैं। आपको सबसे पहले लोन रिकाल नोटिस आता हैं जिसमें पूरी राशि मांगी जाती है। आम तौर पर ऋणी व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता हैं और अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं करता हैं, जो कि करना चाहिए। इसके बाद आर्बिट्रेशन का नोटिस आता हैं जिसमें कहा जाता हैं कि आपके एवं बैंक के बीच विवाद हैं, मध्यस्थ के माध्यम से इसका निराकरण करना चाहते हैं। इसके बाद एक नोटिस आता हैं जिसमें ऋणी व्यक्ति को सोल आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का एक सूचना आता हैं जिसमें कहा जाता हैं कि दोनो के मध्य विवाद के निराकरण के लिए बैंक या कंपनी द्वारा सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया गया हैं। आर्बिट्रेटर के समक्ष बैंक या क्लेमेंट कंपनी स्टैटमैंट ऑफ क्लेम याने की दावा पेश करता हैं और आपको डिफेंस फाईल करने का मौका दिया जाता हैं। इसके बाद साक्ष्य को लिखा जाता हैं और अंतिम बहस को सुना जाता हैं। आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड पारित कर देता हैं।
वास्तव में होता यह हैं कि अक्सर ऋणी व्यक्ति को सीधे आर्बिट्रेटर का अवार्ड मिलता हैं या फिर नोटिस मिलता हैं कि आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पारित कर दिया हैं और जिला एवं सत्र न्यायालय में बैंक या संबंधित कंपनी वसूली की कार्यवाही करने जा रहा है। आर्बिट्रेशन अवार्ड को निरस्त कैसे करवा सकते हैं? यह मुख्य विषय हैं। आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती देने के लिए आपको कानून में समय दिया गया हैं कि सूचना प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर जिला एवं सत्र न्यायालय में धारा 34 में आवेदन पत्र ऋणी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता हैं। विशेष परिस्थिति में 30 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाता हैं। ऋणी व्यक्ति को इसकी संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवष्यक है अन्यथा मामला तकनीकी आधारों पर खारिज होता हैं।
सबसे पहले ऋणी व्यक्ति को चाहिए कि वह सोल आर्बिट्रेटर को एवं कंपनी या बैंक को एक नोटिस जारी करें, जिन आधारों पर ऋणी व्यक्ति आर्बिट्रल अवार्ड को निरस्त करवाना चाहता हैं, उन आधारों को लिखना आवश्यक होता हैं,। इस नियम के तहत धारा 34 (5) का पालन करना आवश्यक है। यदि आप इस तरह का नोटिस नहीं देते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके मामले में पड़ता हैं। आर्बिट्रेटर का अवार्ड निरस्त करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्षेत्राधिकार जो कि ऋण अनुबंध पत्र में लिखा गया हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी हैं। आम तौर पर अनुबंध पत्र में लिखा जाता हैं कि सभी विवादों पर क्षेत्राधिकार किस न्यायालय के अंतर्गत होगा। यदि नहीं लिखा हैं तो सीट ऑफ आर्बिट्रेटर जिस न्यायालय क्षेत्र में स्थित हैं, उसी की जिला एवं सत्र न्यायालय में आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती दी जा सकती हैं। मध्यस्था एवं सुलाह अधिनिमय 1996 में आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती कहाॅ पर दी जा सकती हैं, इस पर सदैव विवाद रहा हैं। सामान्यतः विवादो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार वहाॅ पर होता हैं जहाॅ पर ऋणी व्यक्ति निवास करता हैं, उसी के न्यायालय के क्षेत्र में मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसका समाधान दिया गया हैं कि 3 लाख रूपए तक के मामलों में जिला एवं सत्र न्यायालय सुनवाई करेगा या फिर 3 लाख रूपए से अधिक के मामलों में सुनवाई वाणिज्यिक न्यायालय करेगा जहाॅ पर धारा 34 में आवेदन किया जा सकता हैं।
मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 की धारा 34 के आवेदन के साथ एक शपथ पत्र धारा 34 (5) का दाखिल करना आवश्यक होता हैं जिसमें यह बताया जाता हैं कि बैंक /कंपनी एवं सोल आर्बिट्रेटर को आवेदन पूर्व एक नोटिस दिया गया हैं जिसमें उन आधारों को बताया गया हैं जिस पर आबिट्रेशन अवार्ड को चुनौती दी जानी हैं। इसके साथ में स्थगन आवेदन देना आवश्यक है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड को स्थगित किया जाये। जैसा कि एक वाद दायर होता हैं बाकी की औपचारिकता पूरी की जाती हैं। न्यायालय में आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देने के मात्र 10 आधार होते हैं,। आपको आपका अधिवक्ता यह बता सकता हैं। यदि आपका मामला किसी एक या दो या तीन आधार पर टिक जाता हैं तो धारा 34 का आवेदन सफल हो जाता है एवं आर्बिट्रल अवार्ड निरस्त हो जाता हैं। अक्सर ऋणी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत् समस्याओं को आधार बता कर धारा 34 का आवेदन करता हैं जो कि विधि में मान्य नहीं हैं। मसलन मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था या फिर मेरी दुर्घटना के उपचार में बड़ी धन राशि लग गई थी। एैसे आधार विधित: मान्य नहीं हैं।
पहला विधिमान्य आधार यह हैं कि ऋणी व्यक्ति को अक्षम कर दिया गया था ताकि वह आर्बिट्रेशन कार्यवाही में भाग ना ले सके। दूसरा कि आर्बिट्रेशन अनुबंध अवैध था जिसके आधार पर आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को अपनाया गया था। तीसरा आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं दिया गया, जिसमें आर्बिट्रेशन प्रारंभ की दिनांक एवं नियुक्ति का सूचना पत्र नहीं मिला। चौथा कि एैसी परिस्थितियाॅ जो कि ऋणी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं थी जिसके चलते आप अक्षम हो गए और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। पाॅचवां, आर्बिट्रेशन अनुबंध शर्त या क्षेत्राधिकार के बाहर हैं, एैसी कोई शर्त हैं जो कि अनुबंध के दायरे के बाहर हैं, या विपरीत हैं। मानलों की अनुबंध की 05 शर्तो के अलावा कोई 06 वी परिस्थिति निर्मित हैं जो कि अनुबंध के दायरे के बाहर हैं, मसलन अनुबंध में विवाद की परिस्थिति का उल्लेख हैं, अतिरिक्त कोई अन्य परिस्थिति निर्मित हो गाई हैं। छठवां, अनुबंध में यह नहीं कि कितने आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जायेंगे, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी? आर्बिट्रेशन कहां होगी ? कोई पूर्व सहमति नहीं हैं। सातवां, सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी? सीपीसी लागू होगी अथवा नहीं होगी। धारा 19 कहता हैं कि दोनों पक्ष मिलकर प्रक्रिया तय करेंगे। आठवां, यदि विषय जिसका निर्धारण आर्बिट्रेशन के माध्यम से नहीं किया जा सकता हैं जैसे कि कोई अपराध धटित हुआ हैं, दस्तावेज फर्जी हैं। 09 वाॅ यदि आर्बिट्रेटर भ्रष्ट था, आर्बिट्रेटर बैंक या उसी कंपनी का व्यक्ति हैं। दसवां, जबकि आर्बिट्रेशन अवार्ड प्रांरभ से ही गलत दिखाई दे रहा हैं। न्यायालय को धारा 34 के आवेदन को 01 वर्ष के भीतर निराकरण करना होता हैं।
सामान्यतः न्यायालय में धारा 34 का आवेदन पेश होता हैं तो बैंक या फायनेंस कंपनी ऋणी व्यक्ति से सेटलमेंट करती हैं, कम राशि में सेटलमेंट करती हैं। यदि मामला हाई कोर्ट में लेकर ऋणी व्यक्ति चला जाता हैं तो बहुत कम राशि पर फायनेंस कंपनी सेटलमेंट कर लेती हैं।
बैंक एवं फायनेंस कंपनी से पीड़ितों की संख्या बहुत बड़ी हैं जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हैं। मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 में प्रेक्टिस करने वाला वकील उपलब्ध नहीं हो पाता हैं जिसकी कीमत ऋणी व्यक्ति चुकाता रहता हैं। मानलो कि बैंक ने 09 लाख रूपए का ऋण दिया। ऋणी व्यक्ति ने 02 वर्ष तक ईएमआई अदा करी हैं। बैंक वाहन को जप्त कर लेकर चला गया जो कि गलत था क्योंकि कानून की प्रक्रिया का कोई पालन ही नहीं किया गया। इसके बाद बैंक 49 लाख रूपए की मांग कर रहा हैं। अब ऋणी व्यक्ति क्या करेंगा? बैंक एवं फायनेंस कंपनी के माध्यम से ऋण लेने व्यक्ति को यहा पर सलाह दी जाती हैं कि प्रत्येक नोटिस को प्राप्त करें और योग्य अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस का जवाब दें। अन्य सिविल मामलों की तरह बैंक एवं फायनेंस कंपनी के नोटिस के जवाब नहीं दिए जाते हैं। इसलिए योग्य अधिवक्ता जिसे मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 का ज्ञान हैं, अधिवक्ता की सेवायें लेनी चाहिए। इसका लाभ धारा 34 में आगे जाकर मिलता है।